यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित धर्मपुत्र, भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर है जिसने सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और भारत के विभाजन के विनाशकारी प्रभाव के विषयों को साहसपूर्वक निपटाया है। आचार्य चतुरसेन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित, यह फिल्म यश चोपड़ा के निर्देशन में दूसरी फिल्म है और हिंदी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों के चित्रण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित, जो खुद एक विभाजन उत्तरजीवी थे, फिल्म उस समय के ऐतिहासिक और भावनात्मक निशानों में गहराई से निहित है, जिससे यह विभाजन और हिंदू कट्टरपंथ के उदय को संबोधित करने वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है।
फिल्म 1925 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू होती है, एक ऐसा दौर जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था। यह दिल्ली के दो परिवारों, नवाब बदरुद्दीन परिवार और राय परिवार का अनुसरण करता है, जो एक अटूट बंधन साझा करते हैं। यह निकटता उनके आपसी समर्थन में स्पष्ट है, दोनों परिवार लगभग एक के रूप में रहते हैं। नवाब की बेटी, हुस्न बानो, जावेद के साथ संबंध के बाद विवाह से बाहर गर्भवती हो जाती है, जो बाद में गायब हो जाती है। राय परिवार, विशेष रूप से अमृत राय और उनकी पत्नी सावित्री, इस संकट के दौरान उनका समर्थन करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। वे न केवल हुस्न-बानो को जन्म देने में मदद करते हैं, बल्कि उसके बेटे दिलीप को भी गोद लेते हैं, उसे अपने रूप में पालते हैं।
करुणा का यह कार्य राय परिवार द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष और समावेशी आदर्शों को रेखांकित करता है, जो विविधता में एकता के नेहरूवादी दर्शन को दर्शाता है, जिसे यश चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म, धूल का फूल (1959) में खोजा था। धूल का फूल में, कहानी एक मुस्लिम व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक एक नाजायज हिंदू बच्चे की परवरिश करता है। धर्मपुत्र में, विषय एक बिल्कुल विपरीत मोड़ लेता है, जो एक पोषित बच्चे के घृणा के प्रतीक में परिवर्तन में तल्लीन करता है।
जैसे-जैसे कथा आगे बढ़ती है, त्रासदी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नवाब बदरुद्दीन की मृत्यु के साथ होती है। सालों बाद, हुस्न बानो और उनके पति, जावेद, एक बड़े दिलीप को खोजने के लिए राय के घर लौटते हैं। हालाँकि, यह पुनर्मिलन एक परेशान करने वाला मोड़ लेता है। कभी दोनों परिवारों द्वारा पोषित दिलीप एक कट्टर हिंदू कट्टरपंथी बन गया है। वह मुसलमानों के लिए तीव्र घृणा को परेशान करता है, जो चरमपंथी विचारधाराओं से प्रभावित है। यह परिवर्तन कहानी की जड़ बन जाता है, क्योंकि फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि सांप्रदायिकता रिश्तों को कैसे जहर देती है और सामाजिक सद्भाव को बाधित करती है।
शशि कपूर, अपनी पहली वयस्क भूमिका में, दिलीप के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। कट्टरता से भस्म एक युवक का उनका चित्रण द्रुतशीतन और मार्मिक दोनों है। कपूर दिलीप के आंतरिक संघर्ष की बारीकियों को पकड़ते हैं, जो एक प्यार, समावेशी घर में उनकी परवरिश और उनके द्वारा गले लगाए गए विभाजनकारी बयानबाजी के बीच फटा हुआ है। फिल्म का चरमोत्कर्ष, जहां दिलीप उन लोगों का सामना करता है जिन्होंने उसका पालन-पोषण किया, कट्टरता और अंध घृणा के दुखद परिणामों पर प्रकाश डालता है।
एक विशेष उपस्थिति में राजेंद्र कुमार सहित सहायक कलाकार, कथा में गहराई जोड़ते हैं। शशिकला की संक्षिप्त भूमिका भी फिल्म की भावनात्मक तीव्रता में योगदान देती है। एन दत्ता द्वारा रचित संगीत साहिर लुधियानवी द्वारा गीत के साथ, फिल्म के विषयों का पूरक है। धूल का फूल का एक क्लासिक "तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा" जैसे गीत एकता और मानवता की आवश्यकता पर जोर देते हुए गहराई से गूंजते हैं।
धर्मपुत्र केवल व्यक्तिगत संबंधों की कहानी नहीं है, बल्कि विभाजन से पहले और बाद के भारत के सामाजिक-राजनीतिक माहौल पर एक व्यापक टिप्पणी है। यश चोपड़ा ने व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से आपस में तालमेल बिठाया है, जिससे फिल्म अशांत समय का प्रतिबिंब बन गई है। विभाजन का चित्रण विशेष रूप से हड़ताली है, जो राष्ट्र के विभाजन के साथ अराजकता, हिंसा और नुकसान को पकड़ता है। हिंदू कट्टरपंथ को संबोधित करने में फिल्म का साहस सराहनीय है, जो आज भी एक संवेदनशील विषय है। यह दर्शकों को सांप्रदायिक घृणा और इसके नतीजों के बारे में असहज सच्चाई का सामना करने की चुनौती देता है।
फिल्म अंध राष्ट्रवाद की आलोचना के रूप में भी काम करती है और हिंसा को सही ठहराने के लिए इसे किस तरह से हेरफेर किया जा सकता है। दिलीप के सांप्रदायिक उत्साह में परिवर्तन को एक अलग घटना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि सामाजिक प्रभावों और राजनीतिक एजेंडे के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से, धर्मपुत्र समुदायों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है।
9 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, फिल्म को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इसकी प्रभावशाली कहानी और सामाजिक प्रासंगिकता का एक वसीयतनामा था। हालांकि, इसकी आलोचनात्मक प्रशंसा के बावजूद, धर्मपुत्र ने व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं की, संभवतः इसके हार्ड-हिटिंग विषयों और दर्शकों के बीच पैदा होने वाली असुविधा के कारण। फिर भी, इसकी विरासत एक अग्रणी काम के रूप में बनी हुई है, जिसने मुख्यधारा के सिनेमा द्वारा अक्सर अनदेखा किए गए मुद्दों को संबोधित करने का साहस किया।
पूर्वव्यापी में, धर्मपुत्र भारतीय सिनेमाई इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इसने अधिक सामाजिक रूप से जागरूक कहानी कहने का मार्ग प्रशस्त किया, यश चोपड़ा की संवेदनशीलता और गहराई के साथ जटिल विषयों से निपटने की क्षमता को प्रदर्शित किया। फिल्म की धार्मिक पहचान, सांप्रदायिक सद्भाव और कट्टरता की मानवीय लागत की खोज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1961 में थी। व्यक्तिगत संबंधों और समाज पर घृणा के विनाशकारी प्रभाव का चित्रण करके, धर्मपुत्र तेजी से विभाजित दुनिया में एकता और करुणा की आवश्यकता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करना जारी रखता है।

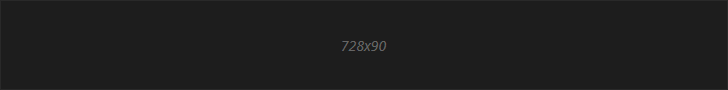









0 Comments